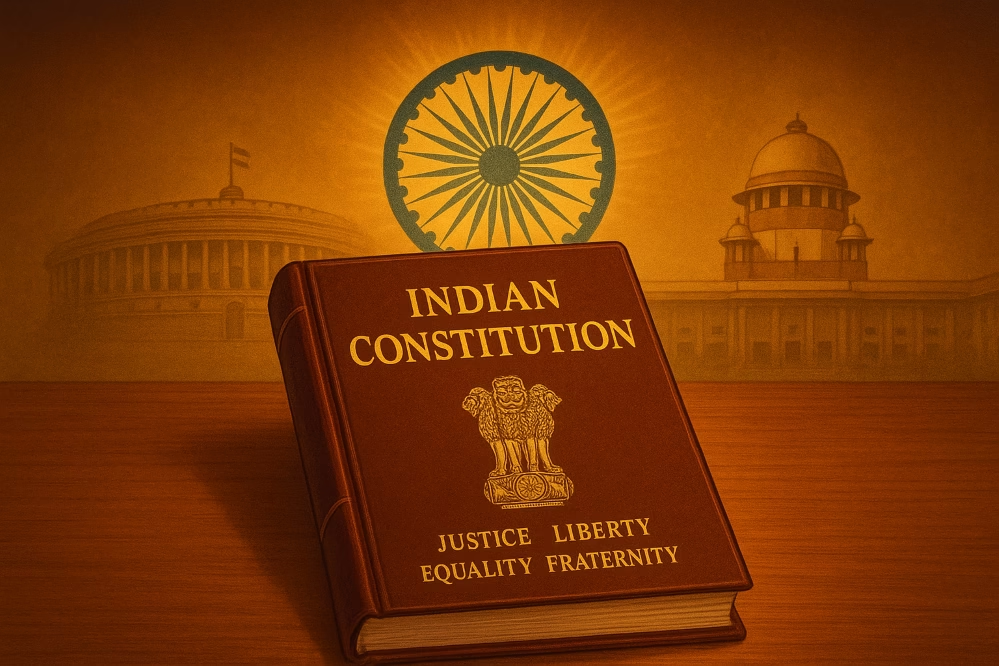भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों का एक जीवंत प्रतीक है। यह वह सर्वोच्च विधि (Supreme Law) है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन के ढांचे और नागरिकों के मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करती है। यह राष्ट्र की आत्मा है, जो हमें एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मार्गदर्शन करती है।
इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके सदस्यों ने लगभग तीन वर्षों (2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन) के अथक परिश्रम और गहन विचार-विमर्श के बाद इस महान ग्रंथ को तैयार किया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने इसके निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें ‘भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार’ कहा जाता है। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिस दिन भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना।
Table of Contents
संविधान की आत्मा: प्रस्तावना
संविधान की मूल भावना और दर्शन उसकी प्रस्तावना (Preamble) में निहित है। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की) और बंधुता (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली) को सुरक्षित करने का संकल्प लेती है।
संरचना और मुख्य विशेषताएँ
अपनी संरचना में, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो आज संशोधनों के बाद बढ़कर लगभग 448 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इसकी विशालता का कारण भारत की भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक जटिलताएँ और केंद्र तथा राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान का होना है।
भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। इसके कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत और कुछ अन्य के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
शासन के स्तंभ और नागरिक अधिकार
यह शासन के तीन स्तंभों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका – की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। साथ ही, यह नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों की रूपरेखा भी तय करता है। इसके तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं:
- मूल अधिकार (भाग 3): ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य की मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।
- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व (भाग 4): ये वे आदर्श हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके।
- मूल कर्तव्य (भाग 4A): ये वे कर्तव्य हैं जो प्रत्येक नागरिक से राष्ट्र के प्रति अपेक्षित हैं।
इसकी विशालता और जटिलता को देखते हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए इसके प्रत्येक भाग, अनुच्छेद और अनुसूची को गहराई से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे दिया गया विस्तृत विवरण इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है कि संविधान के हर एक प्रावधान को सरलता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जा सके, जिससे यह न केवल एक परीक्षा का विषय लगे, बल्कि एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज़ के रूप में समझ में आए जो हमारे राष्ट्र का संचालन करता है।
भाग 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and its Territory)
यह भाग भारत की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें 4 अनुच्छेद हैं।
अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
- (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
- विवरण: यह खंड देश के दो नाम – ‘भारत’ और ‘इंडिया’ – को आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है। यहाँ “राज्यों का संघ” (Union of States) वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, न कि “राज्यों का परिसंघ” (Federation of States)। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, इसके दो अर्थ हैं:
- भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में है।
- किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- विवरण: यह खंड देश के दो नाम – ‘भारत’ और ‘इंडिया’ – को आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है। यहाँ “राज्यों का संघ” (Union of States) वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, न कि “राज्यों का परिसंघ” (Federation of States)। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, इसके दो अर्थ हैं:
- (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
- विवरण: यह स्पष्ट करता है कि भारत में कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, उनकी सूची पहली अनुसूची (First Schedule) में दी गई है।
- (3) भारत के राज्यक्षेत्र में शामिल होंगे:
- (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
- (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और
- (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ।
- विवरण: यह भारत के ‘क्षेत्र’ (Territory of India) को भारत के ‘संघ’ (Union of India) से अधिक व्यापक बनाता है। संघ में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- विवरण: यह अनुच्छेद संसद को दो प्रकार की शक्ति देता है:
- नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति: यह उन राज्यों के लिए है जो पहले से अस्तित्व में हैं (जैसे, सिक्किम का भारत में विलय)।
- नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति: यह उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे।
- संशोधन: 35वें संशोधन (1974) और 36वें संशोधन (1975) के माध्यम से सिक्किम को पहले एक ‘सह-राज्य’ (Associate State) और फिर पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है।
अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
- विवरण: यह अनुच्छेद संसद को किसी भी राज्य के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार देता है:
- (क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना।
- (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना।
- (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटाना।
- (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना।
- (ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना।
- प्रक्रिया: इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसका मत जानने के लिए भेजते हैं। हालाँकि, संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
अनुच्छेद 4: पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ
- विवरण: यह अनुच्छेद दो महत्वपूर्ण बातें कहता है:
- अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून पहली अनुसूची (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा में सीटों का आवंटन) में आवश्यक बदलाव करेगा।
- ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसका अर्थ है कि नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती।
भाग 2: नागरिकता (Citizenship)
यह भाग संविधान के लागू होने के समय (26 जनवरी 1950) भारत का नागरिक कौन होगा, यह तय करता है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। बाद के नागरिकता मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है।
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- विवरण: इस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि:
- वह भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास (Domicile) रखता हो, और
- (क) वह भारत में जन्मा हो, या (ख) उसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या (ग) वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत में मामूली तौर पर निवासी रहा हो।
अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन (migrate) करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- विवरण: यह उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। इसमें शर्त यह है कि यदि वह व्यक्ति (या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई) अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और:
- (a) यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और तब से यहीं रह रहा हो।
- (b) यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो, तो उसे पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा।
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- विवरण: इस अनुच्छेद के अनुसार, कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है: यदि वह व्यक्ति पुनर्वास के लिए परमिट लेकर भारत लौट आता है, तो वह नागरिकता के लिए अनुच्छेद 6(b) के तहत आवेदन कर सकता है।
अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- विवरण: यह उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। यदि वह व्यक्ति (या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई) अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और वह जिस देश में रह रहा है, वहाँ के भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि के पास नागरिक के रूप में पंजीकरण कराता है, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा।
अनुच्छेद 9: विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
- विवरण: यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से एकल नागरिकता के सिद्धांत को स्थापित करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- विवरण: इसके अनुसार, जो कोई भी इन प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, नागरिक बना रहेगा।
अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
- विवरण: यह अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को देता है। यह भविष्य के लिए नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के नियम बनाने का अधिकार है।
- परिणाम: इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) बनाया। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके बताता है: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र के समावेश से। इस अधिनियम में समय-समय पर (जैसे 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 में) कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
भाग 3: मूल अधिकार (Fundamental Rights)
संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35 तक) भारत के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों का वर्णन करता है। इन अधिकारों को ‘मूल’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये अधिकार देश के सामान्य कानूनों से ऊपर हैं और इन्हें सरकार द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। इस भाग को भारत का ‘मैग्ना कार्टा’ (Magna Carta) भी कहा जाता है।
अनुच्छेद 12: ‘राज्य’ की परिभाषा
- विवरण: यह अनुच्छेद मूल अधिकारों के संदर्भ में ‘राज्य’ (State) शब्द को परिभाषित करता है। जब भी इस भाग में ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग होगा, तो उसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे:
- भारत की सरकार और संसद।
- राज्यों की सरकारें और विधानमंडल।
- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी (जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड)।
- अन्य सभी प्राधिकारी (Statutory and Non-statutory authorities) जैसे LIC, ONGC, SAIL आदि।
- महत्व: यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि मूल अधिकार केवल सरकार के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि सरकार के अधीन काम करने वाली विभिन्न इकाइयों के विरुद्ध भी लागू होते हैं।
अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
- विवरण: यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का आधार है। इसके मुख्य प्रावधान हैं:
- (1) संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी कानून, यदि वे मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो उस असंगति की मात्रा तक शून्य (void) होंगे।
- (2) राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो। इस खंड का उल्लंघन करके बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा।
- (3) इस अनुच्छेद में ‘विधि’ (Law) के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना और कानून का बल रखने वाली कोई भी प्रथा या रूढ़ि शामिल है।
- (4) यह अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा। (यह खंड 24वें संशोधन, 1971 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन केशवानंद भारती मामले, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।)
मूल अधिकारों का वर्गीकरण
मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘संपत्ति के अधिकार’ (अनुच्छेद 31) को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं:
1. समता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद 14-18)
अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता
- विवरण: राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता (Equality before the law) या विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of the laws) से वंचित नहीं करेगा।
- विधि के समक्ष समता: यह एक ब्रिटिश अवधारणा है जो नकारात्मक है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति (चाहे वह अमीर हो या गरीब, अधिकारी हो या आम नागरिक) कानून से ऊपर नहीं है।
- विधियों का समान संरक्षण: यह एक अमेरिकी अवधारणा है जो सकारात्मक है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
- (1) राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- (2) कोई भी नागरिक इन आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से, या कुओं, तालाबों, सड़कों आदि के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।
- (3) अपवाद: यह अनुच्छेद राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है (जैसे, महिलाओं के लिए आरक्षण)।
- (4) अपवाद (पहला संशोधन, 1951): यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SC/ST सहित) के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देता है (जैसे, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण)।
- (5) अपवाद (93वां संशोधन, 2005): यह राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) सहित सभी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- (1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
- (2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार के लिए अपात्र नहीं होगा या उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- (3) अपवाद: संसद कानून बनाकर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ‘निवास’ की शर्त लगा सकती है।
- (4) अपवाद: राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत
- विवरण: यह “अस्पृश्यता” का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा।
- कार्यान्वयन: इसी अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया। बाद में, इसे और कठोर बनाने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भी बनाया गया।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
- (1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
- (2) भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
- (3) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
- विवरण: यह अनुच्छेद ब्रिटिश शासन के दौरान दी जाने वाली वंशानुगत उपाधियों (जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान) को समाप्त करता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उपाधि नहीं माने जाते हैं।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19-22)
यह अधिकार लोकतांत्रिक समाज की नींव है। यह नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है।
अनुच्छेद 19: वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
- विवरण: यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है:
- (1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression)।
- (1)(b) शांतिपूर्वक और निरायुध (बिना हथियार के) सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
- (1)(c) संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता (सहकारी समिति शब्द 97वें संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया)।
- (1)(d) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (घूमने) की स्वतंत्रता।
- (1)(e) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता।
- (1)(g) कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
- मूल अधिकार: मूल रूप से इसमें 7 स्वतंत्रताएँ थीं। 1(f) संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की स्वतंत्रता को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया।
- उचित निर्बंधन (Reasonable Restrictions): ये स्वतंत्रताएँ असीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) में राज्य को इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। ये प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के संबंध में लगाए जा सकते हैं।
अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- विवरण: यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) को, जिसे किसी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है, मनमानी और अतिरिक्त सज़ा से संरक्षण प्रदान करता है। इसके तीन भाग हैं:
- कोई पूर्व-पद-प्रभाव कानून नहीं (No ex-post-facto law): किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस कार्य को करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता हो। साथ ही, उसे अपराध करते समय लागू कानून से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती।
- दोहरे दंड का निषेध (No double jeopardy): किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
- आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (No self-incrimination): किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी (गवाह) होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- विवरण: “किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।”
- व्याख्या: यह सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकारों में से एक है। प्रारंभ में इसकी व्याख्या संकीर्ण थी, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या की। अब इसमें केवल जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इसके तहत कई अधिकार माने गए हैं, जैसे- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार (Right to Privacy), आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार आदि।
- अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (Right to Education)
- संशोधन: इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।
- विवरण: राज्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। इस अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया।
अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
- विवरण: यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए या हिरासत (detention) में लिए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। इसके दो भाग हैं:
- 1. साधारण कानून के तहत संरक्षण (Punitive Detention):
- (a) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
- (b) उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होगा।
- (c) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।
- 2. निवारक निरोध कानून के तहत संरक्षण (Preventive Detention):
- यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में लिया जाता है।
- (a) ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों) इसकी अनुमति न दे।
- (b) निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन (representation) करने का अवसर दिया जाएगा।
- 1. साधारण कानून के तहत संरक्षण (Punitive Detention):
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) (अनुच्छेद 23-24)
अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
- विवरण: यह अनुच्छेद मानव के अवैध व्यापार (विशेषकर महिलाओं और बच्चों की खरीद-फरोख्त), बेगार (बिना भुगतान के जबरन काम कराना) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।
- अपवाद: राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा (जैसे सैन्य सेवा) लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
- विवरण: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी जोखिम भरे काम (जैसे निर्माण कार्य या रेलवे) में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28)
अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- विवरण: सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के अंग के रूप में माना जाता है।
- प्रतिबंध: यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है।
अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- विवरण: प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination) या उसके किसी भी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे:
- (a) धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना।
- (b) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना।
- (c) चल और अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व रखना।
- (d) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना।
अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
- विवरण: किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कर (Tax) का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के रखरखाव के लिए व्यय की जाती है। राज्य कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म के उत्थान पर खर्च नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
- (1) राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- (2) हालाँकि, यदि कोई संस्थान किसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुआ है जिसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो वहाँ यह लागू नहीं होगा।
- (3) राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने (या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने) इसके लिए सहमति न दी हो।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) (अनुच्छेद 29-30)
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
- (1) भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
- (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- (1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- (2) राज्य, आर्थिक सहायता देने में, किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) (अनुच्छेद 32)
अनुच्छेद 32: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
- विवरण: यह अनुच्छेद मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा था, क्योंकि इसके बिना अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते।
- रिट (Writs): सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): “शरीर को प्रस्तुत करो”। यह गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है।
- परमादेश (Mandamus): “हम आदेश देते हैं”। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है।
- प्रतिषेध (Prohibition): “रोकना”। यह किसी ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले पर सुनवाई करने से रोकने के लिए जारी की जाती है।
- उत्प्रेषण (Certiorari): “प्रमाणित होना या सूचित करना”। यह किसी ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत से किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या उसके निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
- अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto): “किस अधिकार से”। यह किसी व्यक्ति को यह बताने के लिए जारी की जाती है कि उसने किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण किया है।
अनुच्छेद 33, 34, 35:
- अनुच्छेद 33: संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके।
- अनुच्छेद 34: जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू हो, तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 35: कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को देता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं।
भाग 4: राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy – DPSP)
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उल्लेख है। यह अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये तत्त्व देश में एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना के लिए वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों के विपरीत, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (non-justiciable) नहीं हैं, यानी इनके उल्लंघन पर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता।
अनुच्छेद 36: परिभाषा
- विवरण: इस भाग के लिए ‘राज्य’ शब्द का वही अर्थ है, जो भाग 3 (मूल अधिकार) के अनुच्छेद 12 में है। इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल तथा सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं।
अनुच्छेद 37: इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
- विवरण: यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि इस भाग के उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। किंतु फिर भी, इसमें दिए गए तत्त्व देश के शासन में मूलभूत (fundamental) हैं और विधि (कानून) बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण
संविधान में इनका कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
1. समाजवादी सिद्धान्त (Socialist Principles)
ये सिद्धान्त एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
- अनुच्छेद 38: राज्य, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व:
- (a) सभी नागरिकों (पुरुष और स्त्री) को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
- (b) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।
- (c) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।
- (d) पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।
- (e) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
- संशोधन: इसे 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- विवरण: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली इस तरह से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिले, और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा ताकि कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह जाए।
- अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
- अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य सभी कर्मकारों को एक जीवन-निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना।
- संशोधन: इसे भी 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- विवरण: राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।
2. गांधीवादी सिद्धान्त (Gandhian Principles)
ये सिद्धान्त गांधीजी के विचारों और सपनों पर आधारित हैं।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। (इसी के आधार पर 73वां संशोधन किया गया)।
- अनुच्छेद 43: (कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन) राज्य, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों का उन्नयन।
- संशोधन: इसे 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया।
- विवरण: राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
- अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।
3. उदार-बौद्धिक सिद्धान्त (Liberal-Intellectual Principles)
ये सिद्धान्त उदारवाद की विचारधारा पर आधारित हैं।
- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code)। राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 45: छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध।
- संशोधन: 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने इसकी विषय-वस्तु को बदल दिया। पहले इसमें 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात थी, जिसे अब अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। अब यह राज्य को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
- संशोधन: इसे 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य:
- (a) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा।
- (b) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा।
- (c) अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाएगा।
- (d) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा।
भाग 4A: मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)
अनुच्छेद 51A: मूल कर्तव्य
- संशोधन: यह भाग संविधान में मूल रूप से नहीं था। इसे 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया।
- विवरण: भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह:
- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
- देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।
- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
- (86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया) 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
भाग 5: संघ (The Union) (अनुच्छेद 52-151)
यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जो केंद्र सरकार की संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है।
अध्याय 1: कार्यपालिका (The Executive) (अनुच्छेद 52 से 78 तक)
यह अध्याय संघ की कार्यकारी शाखा से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल हैं।
- अनुच्छेद 52: भारत के राष्ट्रपति
- विवरण: यह अनुच्छेद स्थापित करता है कि “भारत का एक राष्ट्रपति होगा।” राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख (Head of State), भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है।
- अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति
- विवरण: संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। वह भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं।
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन
- विवरण: राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (यह प्रावधान 70वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया)।
- (मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।)
- विवरण: राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
- अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
- विवरण: राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विजेता को पूर्ण बहुमत मिले।
- अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति की पदावधि
- विवरण: राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। हालाँकि, वह अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
- अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- विवरण: कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण कर चुका है, वह उस पद के लिए पुनः चुनाव लड़ने के योग्य है। इस पर कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है।
- अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं (योग्यताएं)
- विवरण: राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति को:
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए।
- संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
- विवरण: राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए व्यक्ति को:
- अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
- विवरण: राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
- अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- विवरण: प्रत्येक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है।
- अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- विवरण: राष्ट्रपति को पद से केवल “संविधान का अतिक्रमण” करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि वह सदन अपने कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर देता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि जांच के बाद दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है।
- अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन
- विवरण: राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाना चाहिए। यदि पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग से रिक्त होता है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 63: भारत का उपराष्ट्रपति
- विवरण: यह अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
- विवरण: उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन (ex-officio) सभापति होता है और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है।
- अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य करना
- विवरण: राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
- विवरण: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है।
- अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति की पदावधि – पाँच वर्ष।
- अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन – कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न होगा।
- अनुच्छेद 69: उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ – राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष।
- अनुच्छेद 70: अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन – संसद को यह शक्ति देता है।
- अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय
- विवरण: इनके चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
- विवरण: राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने, बदलने या निलंबित करने की शक्ति है। यह शक्ति सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा और मृत्युदंड पर भी लागू होती है।
- अनुच्छेद 73: संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- विवरण: राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। 44वें संशोधन, 1978 के बाद, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए वे बाध्य हैं।
- अनुच्छेद 75: मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- विवरण: (1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। (3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। (5) कोई मंत्री यदि 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं बनता तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जायेगा।
- अनुच्छेद 76: भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India)
- विवरण: वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, पर मतदान का नहीं।
- अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्य का संचालन
- विवरण: भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं।
- अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
- विवरण: यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराएं।
अध्याय 2: संसद (Parliament) (अनुच्छेद 79 से 122 तक)
यह अध्याय भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था, यानी संसद की संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 79: संसद का गठन
- विवरण: यह अनुच्छेद स्थापित करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। इन सदनों को राज्य सभा (Council of States) और लोक सभा (House of the People) के नाम से जाना जाएगा6। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं, हालांकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते।
- अनुच्छेद 80: राज्य सभा की संरचना
- विवरण: राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से:
- 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
- 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इनका चुनाव संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- विवरण: राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से:
- अनुच्छेद 81: लोक सभा की संरचना
- विवरण: लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं (104वें संशोधन, 2019 के बाद)।
- 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं।
- 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- पहले 2 एंग्लो-इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
- विवरण: लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं (104वें संशोधन, 2019 के बाद)।
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन
- विवरण: प्रत्येक जनगणना के बाद, संसद विधि द्वारा लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का पुनः समायोजन करती है। वर्तमान में यह समायोजन 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थिर रहेगा।
- अनुच्छेद 83: संसद के सदनों की अवधि
- (1) राज्य सभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- (2) लोक सभा का कार्यकाल, यदि पहले भंग न कर दिया जाए, तो उसकी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 84: संसद की सदस्यता के लिए अर्हता (योग्यता)
- विवरण: कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने के योग्य तब होगा जब वह:
- भारत का नागरिक हो।
- राज्य सभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोक सभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- संसद द्वारा बनाई गई कोई अन्य योग्यता रखता हो।
- विवरण: कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने के योग्य तब होगा जब वह:
- अनुच्छेद 85: संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- विवरण: राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत (बुलाते) हैं। किन्हीं दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति सत्र का सत्रावसान (Prorogation) कर सकते हैं और लोक सभा का विघटन (Dissolution) कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 86: सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- विवरण: राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं और किसी लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकते हैं।
- अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- विवरण: राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरम्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और संसद को उसके आह्वान के कारण बताते हैं।
- अनुच्छेद 88: सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
- विवरण: प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, और संसद की किसी भी समिति में, जिसका वह सदस्य नामित किया जाए, बोलें और उसकी कार्यवाहियों में भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।
संसद के अधिकारी (अनुच्छेद 89-98)
- अनुच्छेद 89-92: ये अनुच्छेद राज्य सभा के सभापति (भारत के उपराष्ट्रपति) और उपसभापति के पद, उनके चुनाव, पद रिक्त होने, और शक्तियों से संबंधित हैं। उपसभापति का चुनाव राज्य सभा अपने सदस्यों में से करती है।
- अनुच्छेद 93-96: ये अनुच्छेद लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद, उनके चुनाव, पद रिक्त होने, और शक्तियों से संबंधित हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है।
- अनुच्छेद 97: सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है।
- अनुच्छेद 98: संसद के प्रत्येक सदन का एक पृथक सचिवीय कर्मचारीवृंद (Secretariat) होगा।
कार्य संचालन (अनुच्छेद 99-100)
- अनुच्छेद 99: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- विवरण: संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
- अनुच्छेद 100: सदनों में मतदान और गणपूर्ति (कोरम)
- विवरण: सदनों में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग (1/10) होती है। यदि गणपूर्ति नहीं है, तो अध्यक्ष या सभापति का यह कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दें।
सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications) (अनुच्छेद 101-104)
- अनुच्छेद 101: कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। साथ ही, यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 102: संसद सदस्य होने के लिए अयोग्यता के आधार बताता है, जैसे लाभ का पद धारण करना, विकृतचित्त होना, या दलबदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्य होना।
- अनुच्छेद 103: सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करेंगे।
- अनुच्छेद 104: अयोग्य होते हुए या बिना शपथ लिए सदन में बैठने या मतदान करने पर प्रतिदिन 500 रुपये के दंड का प्रावधान।
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105-106)
- अनुच्छेद 105: संसद सदस्यों को सदन में भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- अनुच्छेद 106: संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं।
विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 107-111)
- अनुच्छेद 107: साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने की प्रक्रिया। कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकता है।
- अनुच्छेद 108: कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- विवरण: जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
- अनुच्छेद 109: धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- विवरण: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद, राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है या सिफारिशों के साथ वापस भेज सकती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है।
- अनुच्छेद 110: “धन विधेयक” की परिभाषा
- विवरण: कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसमें कर लगाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने, और भारत की संचित निधि से व्यय जैसे मामले शामिल होते हैं।
- अनुच्छेद 111: विधेयकों पर अनुमति
- विवरण: दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, या (धन विधेयक को छोड़कर) विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (अनुच्छेद 112-117)
- अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- विवरण: राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं, जिसे आम तौर पर “बजट” कहा जाता है।
- अनुच्छेद 114: विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)
- विवरण: सरकार, भारत की संचित निधि से कोई भी धन तब तक नहीं निकाल सकती जब तक कि संसद विनियोग विधेयक पारित न कर दे।
- अनुच्छेद 116: लेखानुदान (Vote on Account)
- विवरण: बजट प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा अग्रिम रूप से दी गई मंजूरी।
साधारणतया प्रक्रिया (अनुच्छेद 118-122)
- अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- विवरण: संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा।
- अनुच्छेद 121: संसद में चर्चा पर निर्बंधन
- विवरण: उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर।
- अनुच्छेद 122: न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
- विवरण: संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
अध्याय 3: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers of the President) (अनुच्छेद 123)
यह अध्याय राष्ट्रपति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 123: संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- विवरण: जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों (या कोई एक सदन सत्र में न हो) और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकते हैं।
- शक्ति और प्रभाव: इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है।
- सीमाएं:
- प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- संसद के पुनः समवेत होने की तारीख से छह सप्ताह के समाप्त होने पर यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा, यदि संसद इससे पहले इसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित नहीं करती है।
- राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं।
- अधिकतम अवधि: एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि छह महीने और छह सप्ताह हो सकती है (क्योंकि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने हो सकता है)।
अध्याय 4: संघ की न्यायपालिका (The Union Judiciary) (अनुच्छेद 124 से 147 तक)
यह अध्याय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, यानी उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना, संरचना, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- विवरण: यह अनुच्छेद भारत के एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें एक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति (Chief Justice of India – CJI) और, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या नियत नहीं करती, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। (मूल रूप से यह संख्या 7 थी, जिसे समय-समय पर संसद द्वारा बढ़ाया गया है)।
- नियुक्ति: उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जिनसे वह आवश्यक समझें। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति हमेशा मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हैं।
- योग्यता: कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो और:
- (a) किसी उच्च न्यायालय में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या
- (b) किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या
- (c) राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।
- पद से हटाना: उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की है – यानी, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
- अनुच्छेद 125: न्यायाधीशों के वेतन आदि
- विवरण: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 126: कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
- विवरण: जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हों, तो राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 127: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Ad-hoc Judges)
- विवरण: यदि उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति (कोरम) का अभाव हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को (जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो) अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 128: उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
- विवरण: मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो) से उच्चतम न्यायालय की बैठकों में भाग लेने का अनुरोध कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
- विवरण: उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा। इसके दो निहितार्थ हैं:
- इसके निर्णय और कार्यवाहियाँ सार्वकालिक स्मृति और साक्ष्य के लिए रखे जाते हैं और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- इसे अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
- विवरण: उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा। इसके दो निहितार्थ हैं:
- अनुच्छेद 130: उच्चतम न्यायालय का स्थान
- विवरण: उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा। तथापि, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, किसी अन्य स्थान या स्थानों पर भी इसकी बैठकें आयोजित कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 131: उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction)
- विवरण: यह उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों में सीधे सुनवाई करने का अनन्य अधिकार देता है। ये मामले हैं:
- (a) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद।
- (b) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच कोई विवाद।
- (c) दो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद।
- विवरण: यह उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों में सीधे सुनवाई करने का अनन्य अधिकार देता है। ये मामले हैं:
- अनुच्छेद 132-134: ये अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction) से संबंधित हैं, जिसके तहत वह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। यह संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में लागू होता है।
- अनुच्छेद 136: अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत (Special Leave Petition – SLP)
- विवरण: यह उच्चतम न्यायालय को एक असाधारण शक्ति देता है कि वह भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, या आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत दे सकता है (सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर)।
- अनुच्छेद 137: निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन (Judicial Review)
- विवरण: उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
- अनुच्छेद 141: उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
- विवरण: उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।
- अनुच्छेद 142: उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन
- विवरण: यह उच्चतम न्यायालय को “पूर्ण न्याय” करने के लिए असाधारण शक्ति देता है।
- अनुच्छेद 143: उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति (Advisory Jurisdiction)
- विवरण: यदि राष्ट्रपति को लगता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही राष्ट्रपति दी गई राय को मानने के लिए बाध्य हैं।
- अनुच्छेद 145: न्यायालय के नियम, आदि। उच्चतम न्यायालय अपनी कार्यप्रणाली के लिए नियम बना सकता है।
- अनुच्छेद 146: उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अध्याय 5: भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India) (अनुच्छेद 148 से 151 तक)
यह अध्याय भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान, CAG के पद का प्रावधान करता है। CAG भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और लोक वित्त का संरक्षक है।
- अनुच्छेद 148: भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
- विवरण: भारत का एक CAG होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।
- अनुच्छेद 149: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
- विवरण: CAG, भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार तथा प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय की लेखापरीक्षा करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि क्या सरकारी व्यय नियमों और कानूनों के अनुसार हुआ है।
- अनुच्छेद 150: संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
- विवरण: संघ और राज्यों के खातों को किस रूप में रखा जाएगा, यह CAG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- अनुच्छेद 151: संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit Reports)
- विवरण: CAG, संघ के लेखाओं से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। इसी प्रकार, वह किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। संसद में, इन रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) द्वारा की जाती है।
भाग 6: राज्य (The States)
यह भाग अनुच्छेद 152 से 237 तक फैला हुआ है और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर (अब अनुच्छेद 370 के अप्रभावी होने के बाद यह भी लागू है) भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। इसे छह अध्यायों में बांटा गया है।
अध्याय 1: साधारण (General) (अनुच्छेद 152)
- अनुच्छेद 152: परिभाषा
- विवरण: इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है।
- वर्तमान स्थिति: 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को अप्रभावी किए जाने के बाद, यह प्रावधान व्यवहार में अब लागू नहीं होता है और भाग 6 के प्रावधान अन्य राज्यों की तरह जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होते हैं।
अध्याय 2: कार्यपालिका (The Executive) (अनुच्छेद 153 से 167 तक)
यह अध्याय राज्य की कार्यकारी शाखा, यानी राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से संबंधित है।
- अनुच्छेद 153: राज्यों के राज्यपाल (Governors of States)
- विवरण: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हालांकि, 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 के अनुसार, एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति (Executive power of State)
- विवरण: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे।
- अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor)
- विवरण: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। वह केंद्र सरकार के एक नामित व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
- अनुच्छेद 156: राज्यपाल की पदावधि (Term of office of Governor)
- विवरण: राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (during the pleasure of the President) पद धारण करते हैं। सामान्यतः उनका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष का होता है।
- अनुच्छेद 157: राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं (Qualifications)
- विवरण: कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- अनुच्छेद 158: राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
- विवरण: राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- विवरण: प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है।
- अनुच्छेद 160: कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन – राष्ट्रपति, ऐसी किसी भी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेंगे जो वह ठीक समझते हैं।
- अनुच्छेद 161: क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
- विवरण: राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले किसी भी कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, कम करने, बदलने या निलंबित करने की शक्ति है। (ध्यान दें: राज्यपाल को मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा करने या सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।)
- अनुच्छेद 162: राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार – उन विषयों तक जिन पर उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है।
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- विवरण: राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिन मामलों में राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना है, उन मामलों को छोड़कर वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे।
- अनुच्छेद 164: मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।
- (2) मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- (4) कोई मंत्री जो निरंतर छह महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता (Advocate-General for the State)
- विवरण: प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- अनुच्छेद 166: राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
- विवरण: किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी।
- अनुच्छेद 167: राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
- विवरण: यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दें। यह अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के कर्तव्य) के समान है।
अध्याय 3: राज्य का विधान-मंडल (The State Legislature) (अनुच्छेद 168 से 212 तक)
यह अध्याय राज्य की विधायी शाखा से संबंधित है।
- अनुच्छेद 168: राज्यों के विधान-मंडलों का गठन
- विवरण: अधिकांश राज्यों में एक-सदनीय विधानमंडल (Unicameral Legislature) है, जिसमें राज्यपाल और विधान सभा होती है।
- कुछ राज्यों (वर्तमान में 6: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक) में द्वि-सदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature) है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद् (Legislative Council) और विधान सभा (Legislative Assembly) शामिल हैं।
- अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन (Abolition) या सृजन (Creation)
- विवरण: संसद, विधि द्वारा, किसी राज्य में विधान परिषद् का सृजन या उत्सादन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करती है।
- अनुच्छेद 170: विधान सभाओं की संरचना
- विवरण: किसी राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। (अपवाद: गोवा, मिजोरम, सिक्किम)।
- अनुच्छेद 171: विधान परिषदों की संरचना
- विवरण: किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
- सदस्यों का चुनाव विभिन्न स्रोतों से होता है: 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- अनुच्छेद 172: राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
- विवरण: विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। विधान परिषद् एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
- अनुच्छेद 173: राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
- विवरण: विधान सभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद् के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
- अनुच्छेद 174: राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन – राज्यपाल सत्र को आहूत करेंगे। दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा।
- अनुच्छेद 175: सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
- अनुच्छेद 176: राज्यपाल का विशेष अभिभाषण – आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में।
- अनुच्छेद 177: सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार – उन्हें सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, पर मत देने का नहीं (जब तक सदस्य न हों)।
- अनुच्छेद 178: विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180: अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 181: जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 182: विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 183: सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 184: सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 185: जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 186: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 187: राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय
- अनुच्छेद 188: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 189: सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति (कोरम) – गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10।
- अनुच्छेद 190: स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 191: सदस्यता के लिए निरर्हताएं (अयोग्यताएं)
- अनुच्छेद 192: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय – राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, जो वह निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार देंगे।
- अनुच्छेद 193: अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए… बैठने और मत देने के लिए दंड – प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना।
- अनुच्छेद 194: विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि
- अनुच्छेद 195: सदस्यों के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 196: विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
- अनुच्छेद 197: धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन – विधान परिषद् किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है।
- अनुच्छेद 198: धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया – धन विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 199: “धन विधेयक” की परिभाषा
- विवरण: राज्य के संदर्भ में धन विधेयक की परिभाषा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है।
- अनुच्छेद 200: विधेयकों पर अनुमति
- विवरण: जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, या (धन विधेयक को छोड़कर) विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उनके पास एक और विकल्प है – वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 201: विचार के लिए आरक्षित विधेयक
- विवरण: जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं।
- अनुच्छेद 202: वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)
- विवरण: राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के समक्ष उस राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएंगे।
- अनुच्छेद 203: विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 204: विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 205: अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
- अनुच्छेद 206: लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
- अनुच्छेद 207: वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
- अनुच्छेद 208: प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 209: राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा – राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं में, या हिन्दी में, या अंग्रेजी में।
- अनुच्छेद 211: विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन – उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती।
- अनुच्छेद 212: न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
- विवरण: राज्य विधानमंडल की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
अध्याय 4: राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor) (अनुच्छेद 213)
- अनुच्छेद 213: विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
- विवरण: यह अनुच्छेद 123 (राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति) के समान है। जब राज्य का विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी अवधि भी विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह तक होती है।
अध्याय 5: राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States) (अनुच्छेद 214 से 232 तक)
- अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- विवरण: प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
- अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना – इनके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी।
- अनुच्छेद 216: उच्च न्यायालयों का गठन – मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करें।
- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
- विवरण: उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श किया जाता है। न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है।
- अनुच्छेद 218: उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
- अनुच्छेद 219: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान – राज्यपाल के समक्ष।
- अनुच्छेद 220: स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन – कोई स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 221: न्यायाधीशों के वेतन आदि
- अनुच्छेद 222: किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण (Transfer) – राष्ट्रपति द्वारा।
- अनुच्छेद 223: कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 224: अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 224A: उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 225: विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
- अनुच्छेद 226: कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- विवरण: यह उच्च न्यायालयों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति देता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मूल अधिकारों को लागू करने के लिए और “किसी अन्य प्रयोजन के लिए” (for any other purpose) भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। (ध्यान दें: रिट जारी करने की शक्ति के मामले में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) से व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।)
- अनुच्छेद 227: सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति – अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर।
- अनुच्छेद 228: कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण – यदि उच्च न्यायालय को समाधान हो जाता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न है।
- अनुच्छेद 229: उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
- अनुच्छेद 230: उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार
- अनुच्छेद 231: दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।
- अनुच्छेद 232: (7वें संशोधन, 1956 द्वारा निरस्त)।
अध्याय 6: अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) (अनुच्छेद 233 से 237 तक)
- अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
- विवरण: किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाएगी।
- अनुच्छेद 233A: कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
- अनुच्छेद 234: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती – राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से।
- अनुच्छेद 235: अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होगा।
- अनुच्छेद 236: “न्यायिक सेवा” पद की व्याख्या
- अनुच्छेद 237: कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना
भाग 7: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य (The States in Part B of the First Schedule)
- अनुच्छेद 238:
- विवरण: यह भाग और यह अनुच्छेद पहली अनुसूची के ‘भाग ख’ में उल्लिखित राज्यों से संबंधित था, जिनमें पूर्व की रियासतें शामिल थीं (जैसे हैदराबाद, मैसूर, आदि)।
- वर्तमान स्थिति: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के बाद, राज्यों की श्रेणियों (भाग क, ख, ग) को समाप्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इस पूरे भाग 7 और अनुच्छेद 238 को निरस्त (Repealed) कर दिया गया। इसलिए, यह अब संविधान का हिस्सा नहीं है।
भाग 8: संघ राज्यक्षेत्र (The Union Territories)
यह भाग अनुच्छेद 239 से 242 तक फैला है और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
- अनुच्छेद 239: संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
- विवरण: प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। राष्ट्रपति यह कार्य अपने द्वारा नियुक्त एक प्रशासक (Administrator) के माध्यम से करेंगे। इस प्रशासक को उपराज्यपाल (Lieutenant Governor), मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) या किसी अन्य पदनाम से जाना जा सकता है।
- अनुच्छेद 239A: कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन
- विवरण: संसद, विधि द्वारा, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर (370 हटने के बाद) जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधानमंडल या मंत्रिपरिषद, या दोनों का सृजन कर सकती है।
- अनुच्छेद 239AA: दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
- संशोधन: इसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया।
- विवरण:
- इसने संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली को “राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (National Capital Territory of Delhi)” का विशेष दर्जा दिया और यहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) का पदनाम दिया।
- दिल्ली के लिए एक विधान सभा का सृजन किया गया, जिसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे।
- यह विधान सभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बना सकती है, सिवाय लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस (Police) और भूमि (Land) के। इन तीन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो उपराज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह देगी (उन मामलों को छोड़कर जिनमें उन्हें विवेकानुसार कार्य करना है)।
- यदि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी विषय पर मतभेद हो, तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजेंगे।
- अनुच्छेद 239AB: सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
- विवरण: यदि राष्ट्रपति को उपराज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239AA के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
- अनुच्छेद 239B: विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
- विवरण: जब विधानमंडल सत्र में न हो तो उपराज्यपाल (प्रशासक) अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन है।
- अनुच्छेद 240: कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
- विवरण: राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और पुडुचेरी के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम (Regulations) बनाने की शक्ति है।
- अनुच्छेद 241: संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
- विवरण: संसद, विधि द्वारा, किसी भी संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या किसी भी न्यायालय को उस क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। (उदाहरण: दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है)।
- अनुच्छेद 242: (निरस्त) – यह कूर्ग से संबंधित था, जिसे 7वें संशोधन, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
भाग 9: पंचायतें (The Panchayats)
यह भाग अनुच्छेद 243 से 243-O तक है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- अनुच्छेद 243: परिभाषाएँ – इसमें पंचायत, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर आदि जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है।
- अनुच्छेद 243A: ग्राम सभा – ग्राम सभा में गाँव के स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। यह पंचायती राज की नींव है।
- अनुच्छेद 243B: पंचायतों का गठन – प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया जाएगा। (20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट है)।
- अनुच्छेद 243C: पंचायतों की संरचना – पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है।
- अनुच्छेद 243D: स्थानों का आरक्षण – अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। साथ ही, कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- अनुच्छेद 243E: पंचायतों की अवधि, आदि – प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष का होगा।
- अनुच्छेद 243F: सदस्यता के लिए निरर्हताएं (अयोग्यताएं)
- अनुच्छेद 243G: पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व – राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएँ। ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर उन्हें कार्य करने की शक्ति दी जा सकती है।
- अनुच्छेद 243H: पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
- अनुच्छेद 243-I: वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन – राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।
- अनुच्छेद 243J: पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
- अनुच्छेद 243K: पंचायतों के लिए निर्वाचन – पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- अनुच्छेद 243L: संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना
- अनुच्छेद 243M: इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना – यह भाग कुछ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
- अनुच्छेद 243N: विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
- अनुच्छेद 243-O: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक – पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
भाग 9A: नगरपालिकाएँ (The Municipalities)
यह भाग अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और इसने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया।
- अनुच्छेद 243P – 243T: ये अनुच्छेद नगरपालिकाओं की परिभाषा, गठन, संरचना, वार्ड समितियों का गठन और सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। (प्रावधान पंचायतों के समान हैं, जैसे महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण)।
- अनुच्छेद 243U: नगरपालिकाओं की अवधि, आदि – कार्यकाल 5 वर्ष।
- अनुच्छेद 243V: सदस्यता के लिए निरर्हताएं
- अनुच्छेद 243W: नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व – राज्य विधानमंडल उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने की शक्ति दे सकता है। बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों पर उन्हें कार्य करने की शक्ति दी जा सकती है।
- अनुच्छेद 243X: नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति
- अनुच्छेद 243Y: वित्त आयोग – अनुच्छेद 243-I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग ही नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा।
- अनुच्छेद 243Z: नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
- अनुच्छेद 243ZA: नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन – अनुच्छेद 243K के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग ही नगरपालिकाओं के चुनाव भी कराएगा।
- अनुच्छेद 243ZB: संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना
- अनुच्छेद 243ZC: इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
- अनुच्छेद 243ZD: जिला योजना के लिए समिति (District Planning Committee)
- अनुच्छेद 243ZE: महानगर योजना के लिए समिति (Metropolitan Planning Committee)
- अनुच्छेद 243ZF: विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
- अनुच्छेद 243ZG: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
भाग 9B: सहकारी समितियाँ (The Co-operative Societies)
यह भाग अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT तक है। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, जिसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया।
- यह भाग सहकारी समितियों के गठन, उनके सदस्यों के अधिकार, चुनाव, खातों की लेखापरीक्षा और अन्य प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है।
भाग 10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas)
यह भाग अनुच्छेद 244 से 244A तक है और भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- अनुच्छेद 244: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
- विवरण:
- पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे।
- छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे।
- विवरण:
- अनुच्छेद 244A: असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन
- विवरण: संसद, विधि द्वारा, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी राज्य का निर्माण कर सकती है।
भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between the Union and the States)
यह भाग अनुच्छेद 245 से 263 तक फैला है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करता है। इसे दो अध्यायों में बांटा गया है।
अध्याय 1: विधायी संबंध (Legislative Relations) (अनुच्छेद 245-255)
यह अध्याय केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों के वितरण से संबंधित है।
- अनुच्छेद 245: संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
- विवरण: संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य का विधानमंडल उस पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के बाहर के क्षेत्रों पर भी लागू हो सकता है।
- अनुच्छेद 246: संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु
- विवरण: यह अनुच्छेद शक्तियों के वितरण के लिए सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) का आधार है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं:
- सूची I – संघ सूची (Union List): इस सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद के पास है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि शामिल हैं।
- सूची II – राज्य सूची (State List): इस सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। इसमें स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, स्थानीय शासन आदि शामिल हैं।
- सूची III – समवर्ती सूची (Concurrent List): इस सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें शिक्षा, वन, विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा।
- विवरण: यह अनुच्छेद शक्तियों के वितरण के लिए सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) का आधार है। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं:
- अनुच्छेद 248: अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ (Residuary Powers of Legislation)
- विवरण: कोई भी विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है (यानी अवशिष्ट विषय), उस पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद के पास है।
- अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
- विवरण: यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा कानून एक वर्ष तक प्रभावी रहता है।
- अनुच्छेद 250: यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
- विवरण: जब राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू हो, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
- अनुच्छेद 252: दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
- विवरण: यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह संकल्प पारित करते हैं कि संसद उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है।
- अनुच्छेद 253: अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
- विवरण: संसद किसी अन्य देश के साथ की गई किसी भी संधि, करार या अभिसमय को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकती है, भले ही वह विषय राज्य सूची का हो।
अध्याय 2: प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations) (अनुच्छेद 256-263)
- अनुच्छेद 256: राज्यों की और संघ की बाध्यता
- विवरण: प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- अनुच्छेद 257: कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
- विवरण: केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग) के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्देश दे सकती है।
- अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन
- विवरण: संसद, विधि द्वारा, किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।
- अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद् के संबंध में उपबंध (Inter-State Council)
- विवरण: यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्य परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी, तो वह ऐसी परिषद् की स्थापना कर सकते हैं। इसका कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना और साझा हितों के विषयों पर सिफारिशें करना है।
भाग 12: वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)
यह भाग अनुच्छेद 264 से 300A तक फैला है और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, संपत्ति, अनुबंधों और सरकार के खिलाफ मुकदमों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 265: विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
- विवरण: कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा।
- अनुच्छेद 266: भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे (Consolidated Funds and Public Accounts)
- विवरण: सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व (जैसे कर, ऋण) भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं। इस निधि से कोई भी धन संसद की अनुमति (विनियोग अधिनियम द्वारा) के बिना नहीं निकाला जा सकता।
- अनुच्छेद 267: आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)
- विवरण: संसद एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है, जो राष्ट्रपति के अधीन होती है। इसका उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- अनुच्छेद 275: कुछ राज्यों को संघ से अनुदान (Grants from the Union to certain States)
- विवरण: संसद विधि द्वारा उन राज्यों को सहायता अनुदान दे सकती है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए।
- अनुच्छेद 280: वित्त आयोग (Finance Commission)
- विवरण: राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर या पहले एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है।
- अनुच्छेद 300: वाद और कार्यवाहियाँ (Suits and Proceedings)
- विवरण: भारत सरकार “भारत संघ” के नाम से मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 300A: विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
- संशोधन: इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया।
- विवरण: “किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।” यह संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार (पहले अनुच्छेद 31 में था) से घटाकर केवल एक संवैधानिक/कानूनी अधिकार बनाता है।
भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)
यह भाग अनुच्छेद 301 से 307 तक है और पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 301: व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- विवरण: पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध (free) होगा।
- अनुच्छेद 302-304: ये अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को लोक हित में व्यापार और वाणिज्य पर उचित प्रतिबंध (reasonable restrictions) लगाने की शक्ति देते हैं।
भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services under the Union and the States)
यह भाग अनुच्छेद 308 से 323 तक है और लोक सेवाओं (Civil Services) से संबंधित है।
- अनुच्छेद 309: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
- अनुच्छेद 310: संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि – वे राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (during pleasure) पद धारण करते हैं।
- अनुच्छेद 311: संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
- विवरण: यह सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करता है। किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा जो उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का अधीनस्थ हो। साथ ही, उसे अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता।
- अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services)
- विवरण: यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा) का सृजन कर सकती है।
- अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions)
- विवरण: संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) होगा।
- अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कृत्य (Functions) – भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना।
भाग 14A: अधिकरण (Tribunals)
यह भाग अनुच्छेद 323A और 323B से मिलकर बना है। इसे संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के विवादों के त्वरित और विशेषज्ञ न्यायनिर्णयन के लिए प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों की स्थापना करना था।
- अनुच्छेद 323A: प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals)
- विवरण: यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा, प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के लिए उपबंध कर सके।
- कार्यक्षेत्र: ये अधिकरण केवल लोक सेवाओं (Public Services) से संबंधित विवादों और शिकायतों का निपटारा करते हैं। इसमें संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित मामले शामिल हैं।
- स्थापना: इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया। इसके तहत केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal – CAT) और राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक अधिकरणों (State Administrative Tribunals – SATs) की स्थापना की जाती है।
- उद्देश्य: इनका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों के निपटारे में हो रहे विलंब को कम करना और न्यायालयों के बोझ को हल्का करना है।
- अनुच्छेद 323B: अन्य विषयों के लिए अधिकरण (Tribunals for other matters)
- विवरण: यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को अपनी-अपनी विधायी क्षमता के भीतर, निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों के लिए अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति देता है:
- (a) कराधान (Taxation)
- (b) विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात
- (c) औद्योगिक और श्रम विवाद
- (d) भूमि सुधार
- (e) नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा
- (f) संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन
- (g) खाद्य पदार्थों का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति और वितरण।
- अंतर: अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवा मामलों के लिए है और केवल संसद ही अधिकरण बना सकती है, जबकि 323B कई अन्य विषयों को कवर करता है और इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शक्ति प्राप्त है।
- विवरण: यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को अपनी-अपनी विधायी क्षमता के भीतर, निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों के लिए अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति देता है:
भाग 15: निर्वाचन (Elections)
यह भाग अनुच्छेद 324 से 329A तक है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 324: निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
- विवरण: यह अनुच्छेद एक स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की स्थापना करता है।
- शक्तियाँ: संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार कराने और इन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी।
- संरचना: निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करें। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना
- विवरण: यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह एक सार्वभौमिक मतदाता सूची के सिद्धांत को स्थापित करता है।
- अनुच्छेद 326: लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
- विवरण: लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उसे मतदान करने का अधिकार होगा।
- संशोधन: मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था।
- अनुच्छेद 327: विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति
- विवरण: संसद को निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचनों से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। (उदाहरण: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951)।
- अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति
- विवरण: यदि संसद ने कोई प्रावधान नहीं बनाया है, तो राज्य का विधानमंडल भी अपने चुनावों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है।
- अनुच्छेद 329: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
- विवरण: यह अनुच्छेद निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करता है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। चुनाव को केवल एक चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, जो उच्च न्यायालय में दायर की जाती है।
- अनुच्छेद 329A: (निरस्त) – यह प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित था, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions relating to Certain Classes)
यह भाग अनुच्छेद 330 से 342 तक है और अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), आंग्ल-भारतीय समुदाय (Anglo-Indian Community) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 330: लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- विवरण: लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- अनुच्छेद 331: लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- विवरण: यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे।
- वर्तमान स्थिति: 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए यह अब प्रभावी नहीं है।
- अनुच्छेद 332: राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- विवरण: प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- अनुच्छेद 333: राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- विवरण: यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य की विधान सभा में एक आंग्ल-भारतीय सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति देता था, यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। 104वें संशोधन, 2019 द्वारा इस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है।
- अनुच्छेद 334: स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् न रहना
- विवरण: यह प्रावधान करता है कि आरक्षण की व्यवस्था एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी। इस अवधि को समय-समय पर संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है। 104वें संशोधन ने इसे SCs और STs के लिए अगले दस वर्षों (2030 तक) के लिए बढ़ा दिया है।
- अनुChed 335: सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे
- विवरण: संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्तियाँ करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा।
- अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes)
- विवरण: यह एक संवैधानिक निकाय की स्थापना करता है जो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण उपायों की निगरानी करेगा और उनकी शिकायतों की जांच करेगा।
- अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes)
- संशोधन: इसे 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 से अलग करके एक नए अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया।
- विवरण: यह अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग संवैधानिक आयोग की स्थापना करता है, जिसके कार्य अनुसूचित जाति आयोग के समान हैं।
- अनुच्छेद 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes)
- संशोधन: इसे 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- विवरण: यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक संवैधानिक आयोग की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 340: पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
- विवरण: राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें देने हेतु एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। (उदाहरण: काका कालेलकर आयोग, बी.पी. मंडल आयोग)।
- अनुच्छेद 341: अनुसूचित जातियाँ (Scheduled Castes)
- विवरण: राष्ट्रपति, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, (और यदि यह एक राज्य है, तो उसके राज्यपाल से परामर्श के बाद) एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति माना जाएगा।
- अनुच्छेद 342: अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes)
- विवरण: यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रपति को समान शक्ति प्रदान करता है, जैसा अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के लिए करता है।
भाग 17: राजभाषा (Official Language)
यह भाग अनुच्छेद 343 से 351 तक है और संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं, न्यायपालिका की भाषा और भाषा से संबंधित विशेष निर्देशों को निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा
- (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
- (2) संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि (यानी 1965 तक) के लिए, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए इसका प्रयोग पहले किया जा रहा था।
- अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
- विवरण: राष्ट्रपति, संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद हर दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेंगे जो हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग पर सिफारिशें देगा।
- अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ
- विवरण: किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अपना सकता है।
- अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
- विवरण: जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी।
- अनुच्छेद 350A: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ
- विवरण: प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे।
- अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश
- विवरण: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
भाग 18: आपात उपबंध (Emergency Provisions)
यह भाग अनुच्छेद 352 से 360 तक है और देश में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं।
- अनुच्छेद 352: आपात की उद्घोषणा (Proclamation of Emergency)
- विवरण: यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि एक गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (armed rebellion) के कारण संकट में है, तो वह एक उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
- संशोधन (44वां, 1978):
- “आंतरिक अशांति” (internal disturbance) शब्द को “सशस्त्र विद्रोह” से प्रतिस्थापित किया गया, ताकि इसका दुरुपयोग न हो।
- राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब संघ का मंत्रिमंडल (Cabinet) उन्हें लिखित रूप में ऐसा करने की सलाह दे।
- अनुमोदन: उद्घोषणा जारी होने के एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत) से इसका अनुमोदन आवश्यक है।
- अवधि: एक बार अनुमोदित होने पर, यह छह महीने तक जारी रहता है और इसे हर छह महीने में संसदीय अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 353: आपात की उद्घोषणा का प्रभाव
- विवरण: आपातकाल के दौरान, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी भी राज्य को निर्देश देने तक विस्तारित हो जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।
- अनुच्छेद 354: राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना
- विवरण: आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को संशोधित कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 355: संघ का यह कर्तव्य कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे
- विवरण: यह अनुच्छेद केंद्र पर यह कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है।
- अनुच्छेद 356: राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध (राष्ट्रपति शासन)
- विवरण: यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
- अनुमोदन: उद्घोषणा जारी होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है।
- अवधि: एक बार अनुमोदित होने पर, यह छह महीने तक जारी रहता है और इसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 357: अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
- विवरण: राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं।
- अनुच्छेद 358: आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
- विवरण: जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं।
- अनुच्छेद 359: आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
- विवरण: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अन्य मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
- संशोधन (44वां, 1978): यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 360: वित्तीय आपात के बारे में उपबंध (Financial Emergency)
- विवरण: यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
- अनुमोदन: उद्घोषणा जारी होने के दो महीने के भीतर संसद के साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है।
- प्रभाव: इसके तहत केंद्र, राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ और राज्यों के सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी का आदेश दे सकते हैं। (यह भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ है)।
भाग 19: प्रकीर्ण (Miscellaneous)
यह भाग अनुच्छेद 361 से 367 तक है और इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण
- विवरण: राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 361A: संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण।
- अनुच्छेद 363: कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक।
- अनुच्छेद 365: संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव
- विवरण: यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। (यह अनुच्छेद 356 लगाने का एक आधार बन सकता है)।
- अनुच्छेद 366: परिभाषाएँ – इसमें संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों जैसे “आंग्ल-भारतीय”, “अनुसूचित जातियाँ”, “अनुसूचित जनजातियाँ” आदि को परिभाषित किया गया है।
- अनुच्छेद 367: निर्वचन (Interpretation) – यह संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य नियम प्रदान करता है।
भाग 20: संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)
यह भाग केवल एक अनुच्छेद से बना है, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 368: संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
- विवरण: संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़, बदल या निरस्त कर सकती है। संशोधन तीन तरीकों से हो सकता है:
- संसद के साधारण बहुमत द्वारा: (यह तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के बाहर है) जैसे नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता आदि।
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा: यानी, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत। अधिकांश प्रावधान इसी से संशोधित होते हैं।
- संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधान-मंडलों के अनुसमर्थन द्वारा: यह उन प्रावधानों पर लागू होता है जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र-राज्य विधायी शक्तियों का वितरण, सातवीं अनुसूची, स्वयं अनुच्छेद 368 आदि।
- मूल ढांचे का सिद्धांत: केशवानंद भारती मामले (1973) में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के “मूल ढांचे” (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
- विवरण: संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़, बदल या निरस्त कर सकती है। संशोधन तीन तरीकों से हो सकता है:
भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)
यह भाग अनुच्छेद 369 से 392 तक है।
- अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध।
- विवरण: यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था।
- वर्तमान स्थिति: 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसके अधिकांश खंडों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख – में विभाजित कर दिया गया है।
- अनुच्छेद 371 से 371-J: ये अनुच्छेद कुछ राज्यों के लिए उनके पिछड़े क्षेत्रों के विकास, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा या उनकी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। ये राज्य हैं:
- 371: महाराष्ट्र और गुजरात
- 371A: नागालैंड
- 371B: असम
- 371C: मणिपुर
- 371D: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
- 371F: सिक्किम
- 371G: मिजोरम
- 371H: अरुणाचल प्रदेश
- 371I: गोवा
- 371J: कर्नाटक
भाग 22: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (Short title, Commencement, Authoritative text in Hindi and Repeals)
यह संविधान का अंतिम भाग है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है।
- अनुच्छेद 393: संक्षिप्त नाम
- विवरण: इस संविधान का संक्षिप्त नाम “भारत का संविधान” (The Constitution of India) है।
- अनुच्छेद 394: प्रारंभ
- विवरण: यह बताता है कि नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद (5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 आदि) 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हो गए थे, जबकि शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए, जिसे “संविधान के प्रारंभ की तारीख” कहा जाता है।
- अनुच्छेद 394A: हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
- विवरण: यह राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 395: निरसन (Repeals)
- विवरण: इस अनुच्छेद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया, जिससे भारत पूरी तरह से एक संप्रभु गणराज्य बन गया।