भारत का अपवाह तंत्र 🌊 गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और प्रायद्वीपीय नदियों का अनूठा संगम है। जानें जलग्रहण क्षेत्र, नदी द्रोणियाँ, और उनके आर्थिक महत्व के बारे में।
Table of Contents
परिचय: भारत का अपवाह तंत्र क्या है? 🌍
निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जलप्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को भारत का अपवाह तंत्र कहा जाता है। 🚰 यह तंत्र किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, और बहाव की अवधि का परिणाम है।
- नदी की भूमिका: नदी अपने क्षेत्र का जल ढाल के अनुरूप बहाकर ले जाती है और अंत में किसी झील, खाड़ी, या समुद्र में मिल जाती है। 🌊
- जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area): वह क्षेत्र जहाँ से नदी जल ग्रहण करती है। 🗺️
- अपवाह द्रोणी: एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र।
- जल-संभर (Watershed): एक अपवाह द्रोणी को दूसरी से अलग करने वाली सीमा।
- नदी द्रोणी बनाम जल-संभर:
- बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं।
- छोटी नदियों और नालों के क्षेत्र को जल-संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा, जबकि जल-संभर छोटा होता है।
भारत का अपवाह तंत्र देश की प्राकृतिक और आर्थिक संपदा का आधार है। आइए इसके वर्गीकरण और विशेषताओं को विस्तार से जानें! 🚀
भारत का अपवाह तंत्र का वर्गीकरण 📊
भारत का अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 🌄
समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत का अपवाह तंत्र 🌊
- अरब सागर का अपवाह तंत्र:
- कुल अपवाह क्षेत्र का 23%।
- प्रमुख नदियाँ: सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। 🌊
- बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र:
- कुल अपवाह क्षेत्र का 77%।
- प्रमुख नदियाँ: गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि। 🌊
- अलगाव: ये अपवाह तंत्र दिल्ली कटक, अरावली, और सह्याद्रि द्वारा विलग किए गए हैं।
जल-संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर 📏
- प्रमुख नदी द्रोणी: अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किमी से अधिक।
- उदाहरण: गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि (कुल 14 नदी द्रोणियाँ)। 🌄
- मध्यम नदी द्रोणी: अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किमी।
- उदाहरण: कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि (कुल 44 नदी द्रोणियाँ)। 🌊
- लघु नदी द्रोणी: अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किमी से कम।
हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना 📝
हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपनी उत्पत्ति, प्रवाह, और प्रकृति में भिन्न हैं। नीचे तुलनात्मक तालिका दी गई है:
| क्र.सं. | पक्ष | हिमालयी नदी 🌊 | प्रायद्वीपीय नदी 🌋 |
|---|---|---|---|
| 1. | उद्गम | हिमनदों से ढके हिमालय पर्वत 🏔️ | प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि 🌄 |
| 2. | प्रवाह प्रवृत्ति | बारहमासी (हिमनद व वर्षा से जल) 💧 | मौसमी (मानसून वर्षा पर निर्भर) 🌧️ |
| 3. | अपवाह के प्रकार | पूर्ववती व अनुवर्ती; मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप 🗺️ | अध्यारोपित, पुनर्युवनित; अरीय व आयताकार प्रारूप 📏 |
| 4. | नदी की प्रकृति | लंबा मार्ग, उबड़-खाबड़ पर्वतों से गुजरती, अभिशीर्ष अपरदन, मैदानों में विसर्प 🌊 | सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे, निश्चित मार्ग 🛤️ |
| 5. | जलग्रहण क्षेत्र | बहुत बड़ी द्रोणी 🌍 | अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी 📍 |
| 6. | नदी की आयु | युवा, क्रियाशील, घाटियों को गहरा करती हुई ⏳ | प्रौढ़, आधार तल तक पहुँची हुई 🕰️ |
भारत का अपवाह तंत्र: एक अवलोकन 🌟
भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ शामिल हैं, जो तीन प्रमुख भू-आकृतिक इकाइयों (हिमालय, प्रायद्वीप, और मैदानी क्षेत्र) की उद्-विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। 🌄
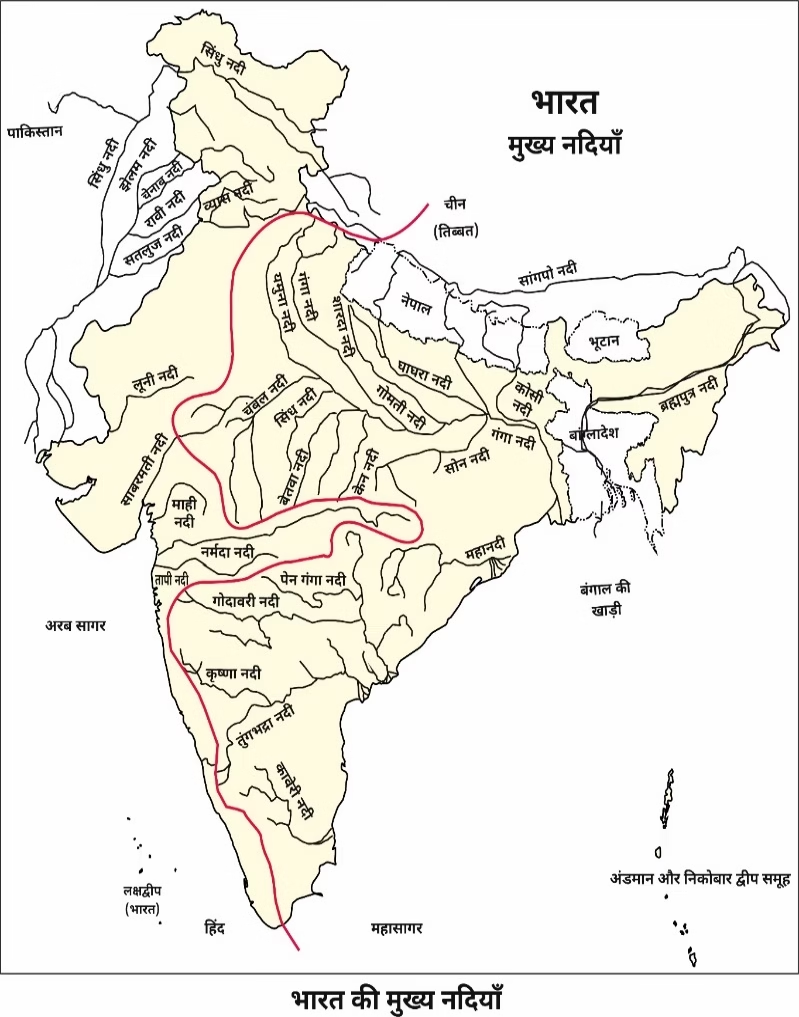
हिमालयी अपवाह तंत्र 🏔️
- विकास: भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित।
- प्रमुख नदियाँ: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।
- विशेषताएँ:
- बारहमासी: हिमनद और वर्षा से जल प्राप्ति। 💧
- महाखड्ड (Gorges): हिमालय के उत्थान के साथ अपरदन द्वारा निर्मित।
- V-आकार की घाटियाँ: पर्वतीय मार्ग में क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात। 🌊
- मैदानी क्षेत्र: निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुंफित वाहिकाएँ, और डेल्टा।
- मार्ग परिवर्तन: टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग, मैदानों में सर्पाकार बहाव। उदाहरण: कोसी नदी (बिहार का शोक)। 😓
- अवसाद: पर्वतों से भारी अवसाद लाकर मैदानों में जमा करती हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध होकर बाढ़ उत्पन्न होती है। 🌪️
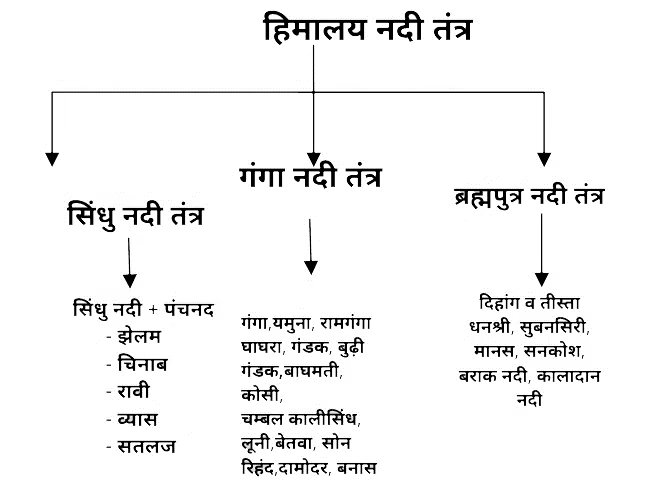
विशाल नदी द्रोणियाँ: हिमालयी नदियाँ 🌊
हिमालय की नदियाँ तीन मुख्य तंत्रों में विभाजित हैं: सिंधु, गंगा, और ब्रह्मपुत्र।
1. सिंधु नदी तंत्र 🌊
- क्षेत्रफल: 11,65,000 वर्ग किमी (भारत में 3,21,289 वर्ग किमी)।
- लंबाई: 2,880 किमी (भारत में 1,114 किमी)।
- उद्गम: तिब्बत में बोखर चू हिमनद (कैलाश पर्वत, 4,164 मीटर)। 🏔️
- नाम: तिब्बत में सिंगी खंबान (शेर मुख)।
- प्रवाह:
- जम्मू-कश्मीर में विशाल गॉर्ज बनाती है।
- लद्दाख, जास्कर, और बलूचिस्तान से गुजरती है।
- पाकिस्तान में अरब सागर में मिलती है।
- सहायक नदियाँ:
- पंचनद: सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास।
- अन्य: शयोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुबरा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, कुर्रम, तोचो, झोब-गोमल।
- सिंधु जल समझौता: भारत 20% जल उपयोग कर सकता है। ⚖️
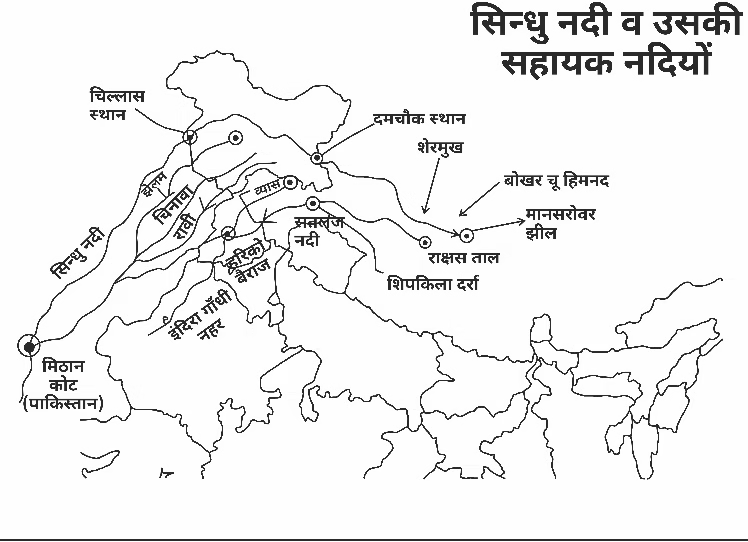
प्रमुख सहायक नदियाँ
- झेलम नदी 🌊
- उद्गम: कश्मीर घाटी में वेरीनाग झरना (पीर पंजाल)।
- विशेषताएँ: वूलर झील (भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील) का निर्माण।
- प्रवाह: श्रीनगर, वूलर झील, और पाकिस्तान में चेनाब में मिलती है।
- परियोजनाएँ: उरी, तुलबुल (जम्मू-कश्मीर)।
- रावी नदी 🌊
- उद्गम: हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा।
- प्रवाह: चंबा घाटी, पीर पंजाल, धौलाधर; पाकिस्तान में चेनाब में मिलती है।
- शहर: जम्मू, लाहौर।
- चेनाब नदी 🌊
- उद्गम: हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा।
- नाम: हिमाचल में चन्द्रभागा (चन्द्र और भागा का संगम)।
- लंबाई: 1,180 किमी।
- परियोजनाएँ: दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार (जम्मू-कश्मीर)।
- व्यास नदी 🌊
- उद्गम: हिमाचल प्रदेश में व्यास कुण्ड (रोहतांग दर्रा, 4,000 मीटर)।
- प्रवाह: कुल्लू घाटी, धौलाधर, पंजाब में सतलज में मिलती है।
- परियोजना: पोंग बाँध (महाराणा प्रताप सागर)।
- सतलज नदी 🌊
- उद्गम: तिब्बत में राक्षस ताल (4,555 मीटर)।
- नाम: तिब्बत में लॉगचेन खंबाब।
- प्रवाह: शिपकी ला दर्रे से भारत में प्रवेश, हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान।
- परियोजना: भाखड़ा-नांगल (गोविन्द सागर)।
सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएँ ⚡️
- बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती: चेनाब नदी, जम्मू-कश्मीर।
- तुलबुल, उरी: झेलम नदी, जम्मू-कश्मीर।
- निम्मो बाजगो: सिंधु नदी, जम्मू-कश्मीर।
- नाथपा-झाकरी: सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश।
- पोंग, चमेरा: व्यास, रावी नदी, हिमाचल प्रदेश।
- इंदिरा गांधी नहर: व्यास, सतलज, राजस्थान-पंजाब-हरियाणा।
2. गंगा नदी तंत्र 🌊
- क्षेत्रफल: 10.63 लाख वर्ग किमी (भारत में 8.6 लाख वर्ग किमी)।
- लंबाई: 2,525 किमी (उत्तर प्रदेश: 1,450 किमी, बिहार: 445 किमी, पश्चिम बंगाल: 520 किमी)।
- उद्गम: उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद (गोमुख, 3,900 मीटर)।
- नाम: उद्गम पर भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा।
- प्रवाह:
- हरिद्वार में मैदान में प्रवेश।
- दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, फिर पूर्व की ओर।
- बांग्लादेश में पद्मा, फिर मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
- सहायक नदियाँ:
- बाएँ तट: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा।
- दाएँ तट: यमुना, सोन, पुनपुन, टोंस।
- शहर: ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, फरक्का, कोलकाता (हुगली), ढाका (पद्मा)।
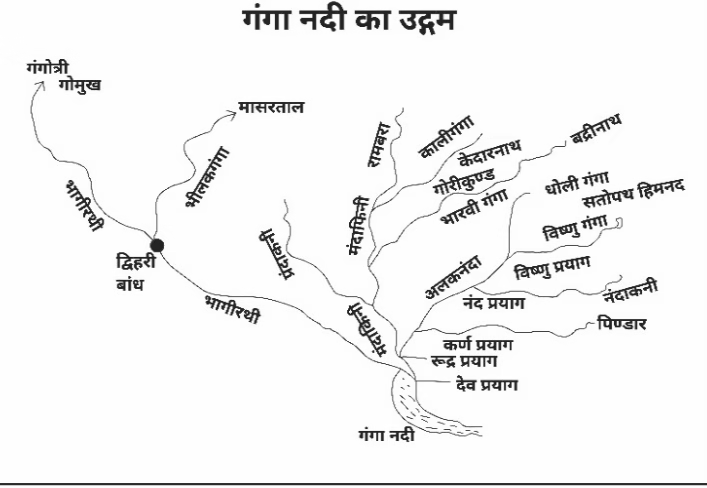
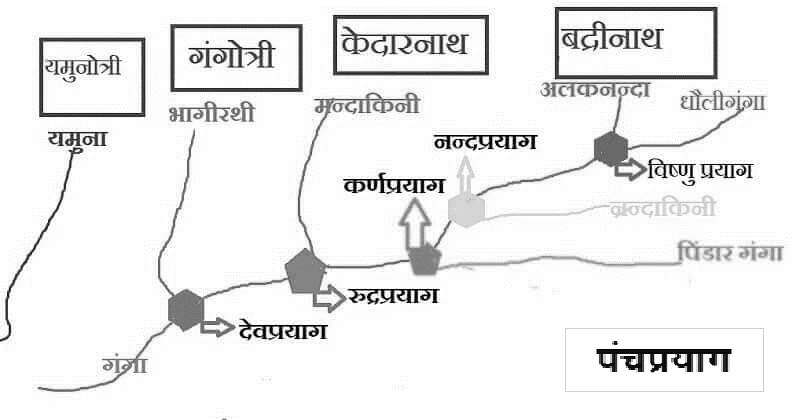
प्रमुख सहायक नदियाँ
- यमुना नदी 🌊
- उद्गम: उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद (बंदर पूँछ)।
- प्रवाह: हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश; प्रयागराज में गंगा से संगम।
- शहर: दिल्ली, मथुरा, आगरा।
- सहायक नदियाँ:
- बाएँ तट: टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा।
- दाएँ तट: चम्बल, सिंध, बेतवा, केन।
- चम्बल नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ियाँ (विंध्य पर्वत)।
- प्रवाह: कोटा, बूँदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर; इटावा में यमुना में मिलती है।
- विशेषताएँ: बीहड़ (उत्खात भूमि) और अवनालिका अपरदन।
- सहायक नदियाँ: क्षिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, बनास।
- रामगंगा नदी 🌊
- उद्गम: उत्तराखंड में नैनीताल (गैरसेन)।
- प्रवाह: शिवालिक, नजीबाबाद, कन्नौज में गंगा में मिलती है।
- विशेषताएँ: जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसके तट पर। 🐅
- गोमती नदी 🌊
- उद्गम: उत्तर प्रदेश में फुल्हर झील (पीलीभीत)।
- प्रवाह: लखनऊ, सुल्तानपुर, गाजीपुर में गंगा में मिलती है।
- घाघरा नदी 🌊
- उद्गम: नेपाल में मापचाचुंगो हिमनद।
- प्रवाह: शारदा नदी से मिलकर छपरा (बिहार) में गंगा में मिलती है।
- सहायक नदियाँ: काली/शारदा, ताप्ती, सरयू।
- गंडक नदी 🌊
- उद्गम: नेपाल में कालीगंगा और त्रिशूल गंगा।
- नाम: नेपाल में नारायणी।
- प्रवाह: चंपारन, सोनपुर (बिहार) में गंगा में मिलती है।
- कोसी नदी 🌊
- उद्गम: नेपाल में गोसाई धाम पर्वत (माउंट एवरेस्ट के उत्तर)।
- नाम: नेपाल में सप्तकोसी।
- विशेषताएँ: बिहार का शोक, मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात। 😓
- कारण: हिमालय के तीव्र ढालों से अवसाद लाकर मैदानों में जमा करती है, जिससे बाढ़।
- प्रवाह: कुरुसेला (बिहार) में गंगा में मिलती है।
- दामोदर नदी 🌊
- उद्गम: छोटा नागपुर पठार।
- प्रवाह: भ्रंश घाटी से होकर हुगली में मिलती है।
- परियोजना: दामोदर घाटी परियोजना (टेनेसी मॉडल)।
- महानंदा नदी 🌊
- उद्गम: दार्जिलिंग हिमालय।
- प्रवाह: फरक्का (पश्चिम बंगाल) में गंगा में मिलती है।
- सिंध नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में मालवा पठार (विदिशा)।
- प्रवाह: उत्तर प्रदेश (जालौन) में यमुना में मिलती है।
- बेतवा नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में विंध्याचल।
- प्रवाह: मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सीमा, हमीरपुर में यमुना में मिलती है。
- परियोजना: माता टीला बाँध।
- केन नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में कैमुर पहाड़ियाँ।
- प्रवाह: बांदा (उत्तर प्रदेश) में यमुना में मिलती है।
- हिण्डन नदी 🌊
- प्रवाह: गाजियाबाद में यमुना में मिलती है।
- तमसा/टोंस नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में विंध्याचल।
- प्रवाह: इलाहाबाद (सिरसा) में गंगा में मिलती है।
- कर्मनाशा नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में त्रिशंकु पहाड़ियाँ।
- प्रवाह: चौसा (बिहार) में गंगा में मिलती है।
- सोन नदी 🌊
- उद्गम: मध्य प्रदेश में अमरकंटक।
- विशेषताएँ: स्वर्ण कण (प्लेसर भण्डार)।
- प्रवाह: दानापुर (बिहार) में गंगा में मिलती है。
- परियोजना: बाण सागर।
- रिहन्द नदी 🌊
- उद्गम: सोन नदी की सहायक।
- परियोजना: रिहन्द बाँध (गोविन्द वल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील)।
- पुनपुन नदी 🌊
- उद्गम: झारखंड (पलामू)।
- प्रवाह: गया (बिहार) में गंगा में मिलती है।
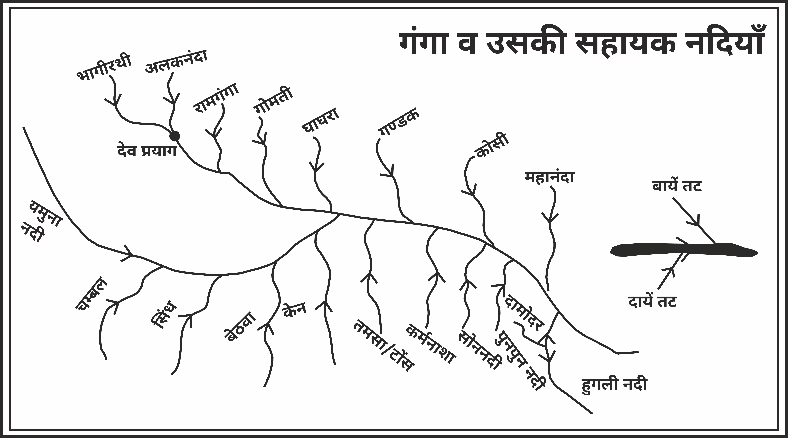
गंगा नदी तंत्र की परियोजनाएँ ⚡️
- टिहरी: उत्तराखंड, भागीरथी (भारत का सबसे ऊँचा बाँध)।
- रामगंगा: उत्तराखंड, रामगंगा (कालागढ़ बाँध)।
- गंडक: बिहार-उत्तर प्रदेश-नेपाल, गंडक।
- कोसी: बिहार-नेपाल, कोसी (बाढ़ नियंत्रण)।
- रिहन्द: उत्तर प्रदेश, रिहन्द।
- बाण सागर: मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश-बिहार, सोन।
- माता टीला: मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश, बेतवा।
- चम्बल: राजस्थान-मध्य प्रदेश, चम्बल (गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर)।
- दामोदर घाटी: झारखंड-पश्चिम बंगाल, दामोदर।
3. ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 🌊
- लंबाई: 2,900 किमी।
- उद्गम: तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमनद (कैलाश पर्वत)।
- नाम:
- तिब्बत में सांग्पो (शोधक)।
- हिमालय में दिहांग।
- असम में ब्रह्मपुत्र।
- बांग्लादेश में जमुना, फिर मेघना।
- प्रवाह:
- तिब्बत में 1,200 किमी पूर्व की ओर।
- अरुणाचल में सादिया से प्रवेश।
- बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
- सहायक नदियाँ:
- बाएँ तट: बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, दिबांग, लोहित।
- दाएँ तट: सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोश, तिस्ता, रागोंसांग्पो।
- विशेषताएँ: माजुली द्वीप (एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप)। 🏝️
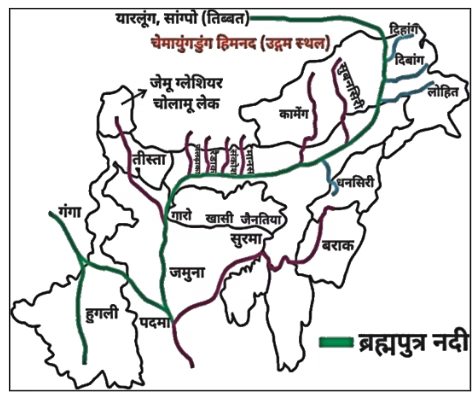
प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 🌋
प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं और मानसून वर्षा पर निर्भर करती हैं। 🌧️
विशेषताएँ 🌊
- जल-विभाजक: पश्चिमी घाट।
- प्रकृति: सुसमायोजित घाटियाँ, आधार तल तक पहुँची हुई।
- मार्ग: सीधा और रैखिक, विसर्पण केवल डेल्टा क्षेत्र में।
- नौकायन: डेल्टा क्षेत्र को छोड़कर नौकायन के लिए अनुपयुक्त।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 🌊
- महानदी:
- उद्गम: छत्तीसगढ़ (सिहावा, रायपुर)।
- लंबाई: 850 किमी।
- क्षेत्रफल: 1.42 लाख वर्ग किमी।
- सहायक नदियाँ: शिवनाथ, हंसदेव, मांड, जोंक, उग, तेल।
- परियोजना: हीराकुण्ड (विश्व का सबसे लंबा बाँध)।
- गोदावरी नदी:
- उद्गम: महाराष्ट्र (नासिक)।
- लंबाई: 1,465 किमी।
- नाम: दक्षिण की गंगा, वृद्धगंगा।
- क्षेत्रफल: 3,12,812 वर्ग किमी।
- सहायक नदियाँ: प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इन्द्रावती, मंजरा, साबरी।
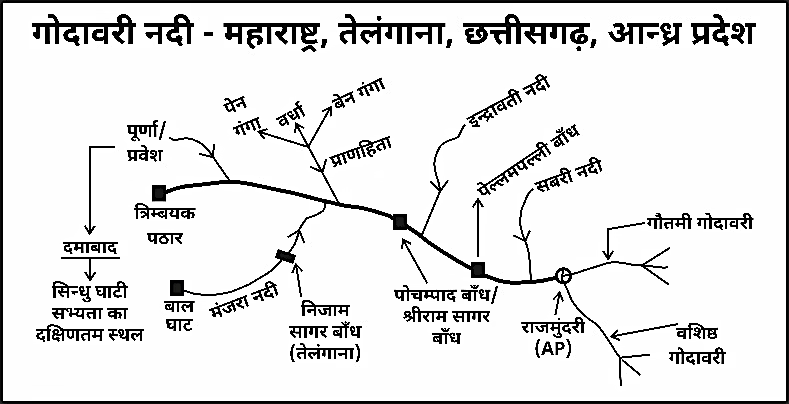
- कृष्णा नदी:
- उद्गम: महाराष्ट्र (महाबलेश्वर)।
- लंबाई: 1,400 किमी।
- क्षेत्रफल: 2,58,948 वर्ग किमी।
- सहायक नदियाँ: कोयना, घाटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरु।
- परियोजनाएँ: अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्री सैलम।
- कावेरी नदी:
- उद्गम: कर्नाटक (ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ)।
- लंबाई: 800 किमी।
- नाम: दक्षिण की गंगा।
- सहायक नदियाँ: हेमावती, लाकेपावनी, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण-तीर्थ, काबीनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती।
- विशेषताएँ: शिवसमुद्रम जलप्रपात, कावेरी जल विवाद।
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 🌊
- झेलम नदी:
- उद्गम: कश्मीर में वेरीनाग झरना।
- प्रवाह: चेनाब में मिलती है।
- चेनाब नदी:
- उद्गम: हिमाचल प्रदेश (बारालाचला दर्रा)।
- लंबाई: 1,180 किमी।
- परियोजनाएँ: सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार।
- रावी नदी:
- उद्गम: हिमाचल प्रदेश (रोहतांग दर्रा)।
- लंबाई: 725 किमी।
- प्रवाह: गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर।
- व्यास नदी:
- उद्गम: हिमाचल प्रदेश (व्यास कुण्ड)।
- लंबाई: 465 किमी।
- प्रवाह: सतलज में मिलती है।
- सतलज नदी:
- उद्गम: तिब्बत (राक्षस ताल)।
- लंबाई: 1,050 किमी।
- परियोजना: भाखड़ा-नांगल।
- लूणी नदी:
- उद्गम: राजस्थान (नाग पहाड़ी, अजमेर)।
- लंबाई: 495 किमी।
- विशेषताएँ: आधी-खारी, आधी-मीठी; कच्छ के रण में विलुप्त।
- सहायक नदियाँ: बाण्डी, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, मिठड़ी, खारी, सागी।
- पश्चिम बनास नदी:
- उद्गम: अरावली (नया सानवरा, सिरोही)।
- प्रवाह: कच्छ के रण में विलुप्त।
- शहर: डीसा।
- साबरमती नदी:
- उद्गम: अरावली (उदयपुर)।
- प्रवाह: खंभात की खाड़ी।
- शहर: अहमदाबाद।
- माही नदी:
- उद्गम: मध्य प्रदेश (विंध्याचल)।
- विशेषताएँ: कर्क रेखा को दो बार काटती है।
- परियोजना: माही बजाज सागर।
- नर्मदा नदी:
- उद्गम: मध्य प्रदेश (अमरकंटक)।
- लंबाई: 1,312 किमी।
- विशेषताएँ: धुआँधार प्रपात, एश्चुअरी।
- परियोजनाएँ: नर्मदा सागर, सरदार सरोवर।
- ताप्ती नदी:
- उद्गम: मध्य प्रदेश (बैतूल)।
- लंबाई: 724 किमी।
- सहायक नदियाँ: पूर्णा, बेघर, गिरना, बोरी, पंझरा, मनेर।
- शहर: सूरत।
- शरावती नदी:
- उद्गम: कर्नाटक (शिमोगा)।
- विशेषताएँ: जोग जलप्रपात।
- पेरियार नदी:
- उद्गम: पश्चिमी घाट (अन्नामलाई)।
- विशेषताएँ: केरल की जीवनरेखा।
- परियोजना: इडुक्की।
प्रायद्वीपीय नदी घाटी परियोजनाएँ ⚡️
- नर्मदा घाटी: मध्य प्रदेश, गुजरात (नर्मदा सागर, सरदार सरोवर)।
- उकाई, काकरापार: गुजरात, तापी।
- माही योजना: मध्य प्रदेश, माही (जमनालाल बजाज सागर)।
- शरावती: कर्नाटक, शरावती (जोग जलप्रपात)।
- इडुक्की: केरल, पेरियार।
- हीराकुण्ड: ओडिशा, महानदी।
- नागार्जुन सागर: तेलंगाना-आंध्र प्रदेश, कृष्णा।
- शिवसमुद्रम: कर्नाटक, कावेरी (भारत की सबसे पुरानी जलविद्युत परियोजना)।
दक्षिण भारत के प्रमुख जलप्रपात 🌊
- महात्मा गांधी (जोग): कर्नाटक, शरावती।
- हुंडरू: झारखंड, स्वर्णरेखा।
- चित्रकुट: छत्तीसगढ़, इन्द्रावती।
- दूधसागर: गोवा-कर्नाटक, मांडवी।
- कुंचीकल: कर्नाटक, वाराही।
हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर 📝
| क्र.सं. | हिमालयी नदियाँ 🏔️ | प्रायद्वीपीय नदियाँ 🌋 |
|---|---|---|
| 1. | हिमनद और वर्षा से जल, सदावाहिनी 💧 | केवल वर्षा से जल, मौसमी 🌧️ |
| 2. | नवीन वलित पर्वत, युवावस्था ⏳ | प्रायद्वीपीय पठार, वृद्धावस्था 🕰️ |
| 3. | बड़ा बेसिन, कम नदियाँ 🌍 | छोटा बेसिन, अधिक नदियाँ 📍 |
| 4. | V-आकार घाटियाँ, गॉर्ज, जलप्रपात 🌊 | चौड़ी घाटियाँ 🛤️ |
| 5. | उच्च जलविद्युत क्षमता, अपूर्ण उपयोग ⚡️ | कम जलविद्युत क्षमता, पूर्ण उपयोग 🔌 |
| 6. | हिमालय और सहायक नदियाँ 🏔️ | प्रायद्वीप और सहायक नदियाँ 🌄 |
| 7. | मैदानों में विसर्पण 🌊 | डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण 📏 |
| 8. | अधिक अवसाद, वृहद मैदान 🌍 | कम अवसाद, सीमित मैदान 📍 |
| 9. | नौकायन के लिए उपयुक्त 🚤 | डेल्टा क्षेत्र में ही नौकायन 🚣 |
| 10. | पूर्ववती और अनुवर्ती नदियाँ 🗺️ | केवल अनुवर्ती नदियाँ 📏 |
निष्कर्ष: भारत के अपवाह तंत्र का महत्व 🌟
भारत का अपवाह तंत्र देश की प्राकृतिक और आर्थिक समृद्धि का आधार है। 🌍 हिमालयी नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु, और ब्रह्मपुत्र बारहमासी जल प्रदान करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी मानसून पर निर्भर हैं। 🌧️ ये नदियाँ कृषि, जलविद्युत, और उद्योगों को समृद्ध करती हैं। 💪
इस तंत्र की विविधता, बाढ़, और मार्ग परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ इसे और भी रोचक बनाती हैं। आइए, इस प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करें। 💧 क्या आप भारत के अपवाह तंत्र के किसी पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करें! 💬






Bohot acchi jankari hai